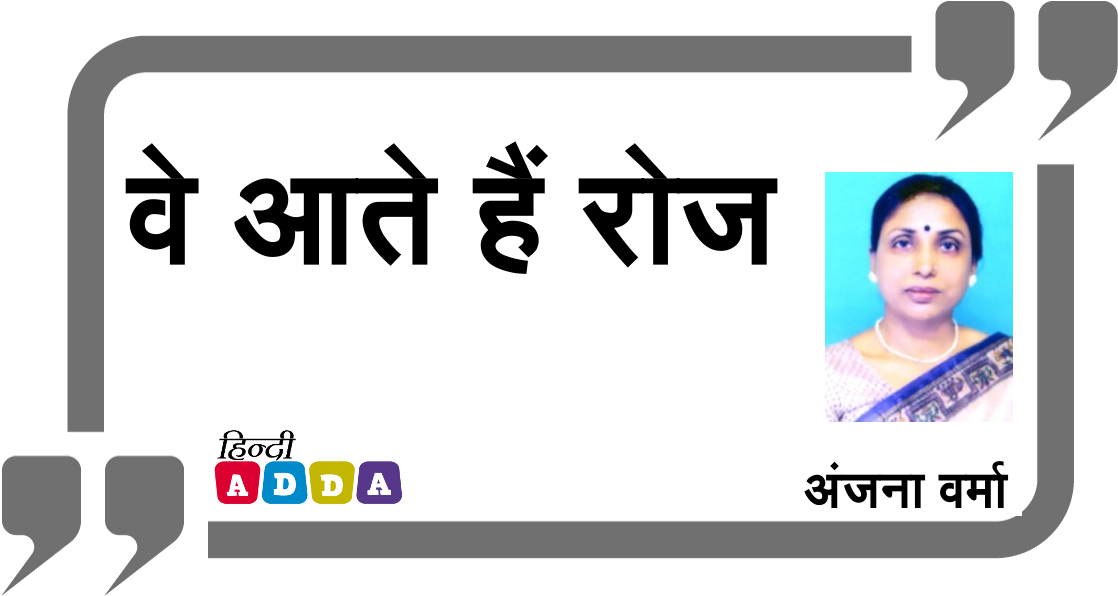वे आते हैं रोज | अंजना वर्मा
वे आते हैं रोज | अंजना वर्मा
वे भी निकलते हैं सुबह-सुबह
टहलने के लिए पार्क में
जो जिंदगी की आधी शताब्दी पूरी कर चुके हैं
निकल आए हैं आगे
कोई कुछ आगे
तो कोई बहुत आगे
और उनमें से अधिकांश ने
खो दिया है अपना आधा अंग
हो गए हैं अकेले और अधूरे
परंतु जिंदगी का संघर्ष
हो गया है दोगुना
टहलते हुए उन्हें कई दोस्त मिल जाते हैं
कोई उनके साथ टहलने लगता है
चलता है साथ-साथ
कदम-से-कदम मिलाते हुए
तो कोई हाय-हैलो कहकर या
कोई उनके साथ सिर्फ एक चक्कर लगाकर ही
थक-हारकर बैठ जाता है
सब कम टहलें या अधिक
बेचैन होकर बैठेंगे इसी बेंच पर
जो बनी हुई है
इन जहाज के पंछियों की शरणस्थली
सबके पास है अपनी-अपनी कहानी
पर सबकी कहानियों के पन्ने भीगे हैं
क्योंकि घर की छत ही टपकने लगी है
दरीचियाँ – अल्मारियाँ रिसने लगी हैं
कहाँ रखें वे अपनी कहानी छुपाकर ?
वे सब अपने कंठों में
कफ की तरह अटके शब्दों को
बाहर निकाल देने के लिए बेचैन हैं
बसेरों में पिए गए धुएँ को निकालकर
ऑक्सीजन भर लेते है फेफड़ों में
आकाश में नजर उठाकर देखते हैं
तो उन्हें अपने दड़बे दिखाई देते हैं
जिनमें जाकर अभी समा जाना है
फिर भी जीने के लिए
थोड़ी मिल चुकी है संजीवनी
जितने भी दिन शेष हों जीवन के
इस हरे-भरे पार्क और इस बेंच के लिए
उनके दिलों से बहुत दुआएँ निकलती हैं
यह जो एक पसरा हुआ मैदान है
यह नहीं है मनुष्य
नहीं है उनका साथी
कि उसके पास कान हैं सुनने के लिए
आँखें है देखने के लिए
हाथ हैं सहलाने के लिए
फिर भी वह उनकी सुनता है
उन्हें देखता है
और मिलता है उनसे ललककर
इसीलिए वे आते हैं
एक अजब उत्साह के साथ
बिला नागा रोज
सुनाते हैं उसे अपनी खामोशी में
कहते हैं उससे वह सब
जो वे नहीं कह सकते किसी से