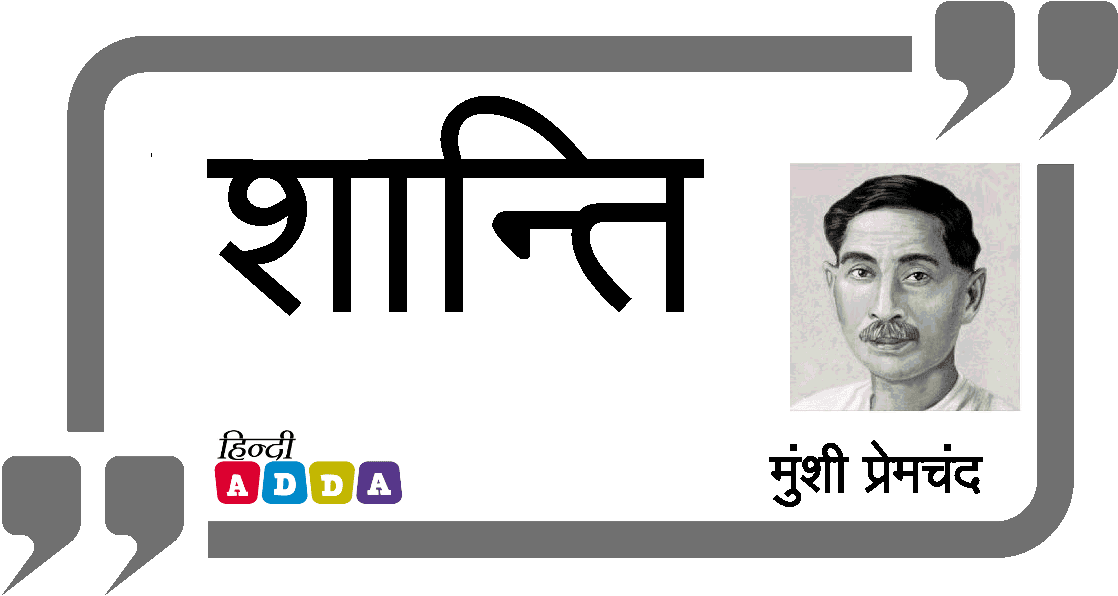जब मै ससुराल आयी, तो बिलकुल फूहड थी। न पहनने-ओढ़ने को सलीका , न बातचीत करने का ढंग। सिर उठाकर किसी से बातचित न कर सकती थीं। ऑंखें अपने आप झपक जाती थीं। किसी के सामने जाते शर्म आती, स्त्रियों तक के सामने बिना घूँघट के झिझक होती थी। मैं कुछ हिन्दी पढ़ी हुई थी; पर उपन्यास, नाटक आदि के पढ़ने में आन्नद न आता था। फुर्सत मिलने पर रामायण पढ़ती। उसमें मेरा मन बहुत लगता था। मै उसे मनुष्य-कृत नहीं समझती थी। मुझे पूरा-पूरा विश्वास था कि उसे किसी देवता ने स्वयं रचा होगा। मै मनुष्यों को इतना बुद्धिमान और सहृदय नहीं समझती थी। मै दिन भर घर का कोई न कोई काम करती रहती। और कोई काम न रहता तो चर्खे पर सूत कातती। अपनी बूढ़ी सास से थर-थर कॉँपती थी। एक दिन दाल में नमक अधिक हो गया। ससुर जी ने भोजन के समय सिर्फ इतना ही कहा—‘नमक जरा अंदाज से डाला करो।’ इतना सुनते ही हृदय कॉँपने लगा। मानो मुझे इससे अधिक कोई वेदना नहीं पहुचाई जा सकती थी।
लेकिन मेरा यह फूहड़पन मेरे बाबूजी (पतिदेव) को पसन्द न आता था। वह वकील थे। उन्होंने शिक्षा की ऊँची से ऊँची डिगरियॉँ पायी थीं। वह मुझ पर प्रेम अवश्य करते थे; पर उस प्रेम में दया की मात्रा अधिक होती थी। स्त्रियों के रहन-सहन और शिक्षा के सम्बन्ध में उनके विचार बहुत ही उदार थे; वह मुझे उन विचारों से बहुत नीचे देखकर कदाचित् मन ही मन खिन्न होते थे; परन्तु उसमें मेरा कोई अपराध न देखकर हमारे रस्म-रिवाज पर झुझलाते थे। उन्हें मेरे साथ बैठकर बातचीत करने में जरा आनन्द न आता। सोने आते, तो कोई न कोई अँग्रेजी पुस्तक साथ लाते, और नींद न आने तक पढ़ा करते। जो कभी मै पूछ बैठती कि क्या पढ़ते हो, तो मेरी ओर करूण दृष्टि से देखकर उत्तर देते—तुम्हें क्या बतलाऊँ यह आसकर वाइल्ड की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मै अपनी अयोग्यता पर बहुत लज्जित थी। अपने को धिक्कारती, मै ऐसे विद्वान पुरूष के योग्य नहीं हूँ। मुझे किसी उजड्ड के घर पड़ना था। बाबूजी मुझे निरादर की दृष्टि से नहीं देखते थे, यही मेरे लिए सौभग्य की बात थी।
एक दिन संध्या समय मैं रामायण पढ़ रही थी। भरत जी रामचंद्र जी की खोज में निकाले थे। उनका करूण विलाप पढ़कर मेरा हृदय गदगद् हो रहा था। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। हृदय उमड़ आता था। सहसा बाबू जी कमरे में आयें। मैने पुस्तक तुरंत बन्द कर दीं। उनके सामने मै अपने फूहड़पन को भरसक प्रकट न होने देती थी। लेकिन उन्होंने पुस्तक देख ली; और पूछा—रामायण है न?
मैने अपराधियों की भांति सिर झुका कर कहा—हॉँ, जरा देख रही थी।
बाबू जी—इसमें शक नहीं कि पुस्तक बहुत ही अच्छी, भावों से भरी हुई है; लेकिन जैसा अंग्रेज या फ्रांसीसी लेखक लिखतें हैं। तुम्हारी समझ में तो न आवेगा, लेकिन कहने में क्या हरज है, योरोप में अजकल ‘स्वाभाविकता’ ( Realism) का जमाना है। वे लोग मनोभावों के उत्थान और पतन का ऐसा वास्तविक वर्णन करते है कि पढ़कर आश्चर्य होता है। हमारे यहॉँ कवियो को पग-पग पर धर्म तथा नीति का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए कभी-कभी उनके भावों में अस्वभाविकता आ जाती है, और यही त्रुटी तुलसीदास में भी है।
मेरी समझ में उस समय कुछ भी न आया। बोली –मेरे लिए तो यही बहुत है, अँग्रेजी पुस्तकें कैसे समझूँ।
बाबू जी—कोई कठिन बात नहीं। एक घंटे भी रोज पढ़ो, तो थोड़े ही समय में काफी योग्यता प्रप्त कर सकती हो; पर तुमने तो मानो मेरी बातें न मानने की सौगंध ही खा ली है। कितना समझाया कि मुझसे शर्म करने की आवश्यकता नहीं, पर तुम्हारे ऊपर असर न पड़ा। कितना कहता हूं कि जरा सफाई से रहा करो, परमात्मा सुन्दरता देता है तो चाहता है कि उसका श्रृंगार भी होता रहे; लेकिन जान पड़ता है, तुम्हारी दृष्टि में उसका कुछ भी मूल्य नहीं ! या शायद तुम समझती हो कि मेरे जैसे कुरूप मनुष्य के लिए तुम चाहे जैसा भी रहो, आवश्यकता से अधिक अच्छी हो। यह अत्याचार मेरे ऊपर है। तुम मुझे ठोंक-पीट कर वैराग्य सिखाना चाहती हो। जब मैं दिन-रात मेहनत करके कमाता हूँ तो स्व-भावत:- मेरी यह इच्छा होती है कि उस द्रव्य का सबसे उत्तम व्यय हो। परन्तु तुम्हारा फूहड़पन और पुराने विचार मेरे सारे परिश्रम पर पानी फेर देते है। स्त्रियाँ केवल भोजन बनाने, बच्चे पालने, पति सेवा करने और एकादशी व्रत रखने के लिए नहीं है, उनके जीवन का लक्ष्य इससे बहुत ऊँचा है। वे मनुष्यों के समस्त सामाजिक और मानसिक विषयों में समान रूप से भाग लेने की अधिकारिणी हैं। उन्हे भी मनुष्यों की भांति स्वतंत्र रहने का अधिकार प्राप्त है। मुझे तुम्हारी यह बंदी-दशा देखकर बड़ा कष्ट होता है। स्त्री पुरष की अर्द्धागिनी मानी गई है; लेकिन तुम मेरी मानसिक और सामाजिक, किसी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकतीं। मेरा और तुम्हारा धर्म अलग, आचार-विचार अलग, आमोद-प्रमोद के विषय अलग। जीवन के किसी कार्य में मुझे तुमसे किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती। तुम स्वयं विचार सकती हो कि ऐसी दशा में मेरी जिंदगी कैसी बुरी तरह कट रही है।
बाबू जी का कहना बिलकुल यथार्थ था। मैं उनके गले में एक जंजीर की भांति पड़ी हुई थी। उस दिन से मैने उन्हीं के कहें अनुसार चलने की दृढृ प्रतिज्ञा करली, अपने देवता को किस भॉँति अप्रसन्न करती?
यह तो कैसे कहूँ कि मुझे पहनने-ओढ़ने से प्रेम न था, और उतना ही था, जितना दूसरी स्त्रियों को होता है। जब बालक और वृद्ध तक श्रृंगार पसंद करते है, तों मैं युवती ठहरी। मन भीतर ही भीतर मचल कर रह जाता था। मेरे मायके में मोटा खाने और मोटा पहनने की चाल थी। मेरी मॉँ और दादी हाथों से सूत कातती थीं; और जुलाहे से उसी सूत के कपड़े बुनवा लिए जाते थे। बाहर से बहुत कम कपड़े आते थे। में जरा महीन कपड़ा पहनना चाहतीं या श्रृगार की रूची दिखाती तो अम्मॉँ फौरन टोकतीं और समझाती कि बहुत बनाव-सवॉँर भले घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता। ऐसी आदत अच्छी नहीं। यदि कभी वह मुझे दर्पण के सामने देख लेती, तो झिड़कने लगती; परन्तु अब बाबूजी की जिद से मेरी यह झिझक जाती रही। सास और ननदें मेरे बनाव-श्रृंगार पर नाक-भौं सिकोड़ती; पर मुझे अब उनकी परवाह न थी। बाबूजी की प्रेम-परिपूर्ण दृष्टि के लिए मै झिड़कियां भी सह सकती थी। अब उनके और मेरे विचारों में समानता आती जाती थी। वह अधिक प्रसन्नचित्त जान पड़ते थे। वह मेरे लिए फैसनेबुल साड़ियॉँ, सुंदर जाकटें, चमकते हुए जूते और कामदार स्लीपरें लाया करते; पर मैं इन वस्तुओं को धारण कर किसी के सामने न निकलती, ये वस्त्र केवल बाबू जी के ही सामने पहनने के लिए रखे थे। मुझे इस प्रकार बनी-ठनी देख कर उन्हे बड़ी प्रसन्नता होती थी। स्त्री अपने पति की प्रसन्नता के लिए क्या नहीं कर सकती। अब घर के काम-काज से मेरा अधिक समय बनाव-श्रृंगार तथा पुस्तकावलोकन में ही बीतने लगा। पुस्तकों से मुझे प्रेम हाने लगा था।
यद्यपि अभी तक मै अपने सास-ससुर का लिहाज करती थी, उनके सामने बूट और गाउन पहन कर निकलने का मुझे साहस न होता था, पर मुझे उनकी शिक्षा-पूर्ण बाते न भांति थी। मैं सोचती, जब मेरा पति सैकड़ों रूपये महीने कमाता है तो घर में चेरी बनकर क्यों रहूँ? यों अपनी इच्छा से चाहे जितना काम करूँ, पर वे लोग मुझे आज्ञा देने वाले कौन होते हैं? मुझमें आत्मभिमान की मात्रा बढ़ने लगी। यदि अम्मॉँ मुझे कोई काम करने को कहतीं, तो तैं अदबदा कर टाल जाती। एक दिन उन्होनें कहा—सबेरे के जलपान के लिए कुछ दालमोट बना लो। मैं बात अनसुनी कर गयी। अम्मॉँ ने कुछ देर तक मेरी राह देखी; पर जब मै अपने कमरे से न निकली तों उन्हे गुस्सा हो आया। वह बड़ी ही चिड़चिड़ी प्रकृति की थी। तनिक-सी बात पर तुनक जाती थीं। उन्हे अपनी प्रतिष्ठा का इतना अभिमान था कि मुझे बिलकुल लौंडी समझती थीं। हॉँ, अपनी पुत्रियों से सदैव नम्रता से पेश आतीं; बल्कि मैं तो यह कहूँगी कि उन्हें सिर चढ़ा रखा था। वह क्रोध में भरी हुई मेरे कमरे के द्वार पर आकर बोलीं—तुमसे मैंने दाल—मोट बनाने को कहा था, बनाया?
मै कुछ रूष्ट होकर बोली—अभी फुर्सत नहीं मिली।
अम्मॉँ—तो तुम्हारी जान में दिन-भर पड़े रहना ही बड़ा काम है! यह आजकल तुम्हें हो क्या गया है? किस घमंड में हो? क्या यह सोचती हो कि मेरा पति कमाता है, तो मै काम क्यों करूँ? इस घमंड में न भूलना! तुम्हारा पति लाख कमाये; लेकिन घर में राज मेरा ही रहेगा। आज वह चार पैसे कमाने लगा है, तो तुम्हें मालकिन बनने की हवस हो रही है; लेकिन उसे पालने-पोसने तुम नहीं आयी थी, मैंने ही उसे पढ़ा-लिखा कर इस योग्य बनाया है। वाह! कल को छोकरी और अभी से यह गुमान।
मैं रोने लगी। मुँह से एक बात न निकली। बाबू जी उस समय ऊपर कमरे में बैठे कुछ पढ़ रहे थे। ये बातें उन्होंने सुनीं। उन्हें कष्ट हुआ। रात को जब वह घर आये तो बोले—देखा तुमने आज अम्मॉँ का क्रोध? यही अत्याचार है, जिससे स्त्रियों को अपनी जिंदगी पहाड़ मालूम होते लगत है। इन बातों से हृदय में कितनी वेदना होती है, इसका जानना असम्भव है। जीवन भार हो जाता है, हृदय जर्जर हो जाता है और मनुष्य की आत्मोन्नति उसी प्रकार रूक जाती है जैसे जल, प्रकाश और वायु के बिना पौधे सूख जाते है। हमारे घरों में यह बड़ा अंधेर है। अब मैं उनका पुत्र ही ठहरा। उनके सामने मुँह नहीं खोल सकूँगा। मेरे ऊपर उनका बहुत बड़ा अधिकार है। अतएव उनके विरुद्ध एक शब्द भी कहना मेरे लिये लज्जा की बात होगी, और यही बंधन तुम्हारे लिए भी है। यदि तुमने उनकी बातें चुपचाप न सुन ली होतीं, तो मुझे बहुत ही दु:ख होता। कदाचित् मैं विष खा लेता। ऐसी दशा में दो ही बातें सम्भव है, या तो सदैव उनकी घुड़कियों-झिड़कियों को सहे जाओ, या अपने लिए कोई दूसरा रास्ता ढूढ़ो। अब इस बात की आशा करना कि अम्मॉँ के सवभाव में कोई परिवर्तन होगा, बिलकुल भ्रम है। बोलो, तुम्हें क्या स्वीकार है।
मैंने डरते डरते कहा—आपकी जो आज्ञा हो, वह करें। अब कभी न पढूँ-लिखूँगी, और जो कुछ वह कहेंगी वही करूँगी। यदि वह इसी में प्रसन्न हैं तो यही सही। मुझे पढ़-लिख कर क्या करना है?
बाबूजी –पर यह मैं नहीं चाहती। अम्मॉँ ने आज आरम्भ किया है। अब रोज बढ़ती ही जायँगी। मैं तुम्हें जितनी ही सभ्य तथा विचार-शील बनाने की चेष्टा करूँगा, उतना ही उन्हें बुरा लगेगा, और उनका गुस्सा तुम्हीं पर उतरेगा। उन्हें पता नहीं जिस अबहवा में उन्होंने अपनी जिनदगी बितायी है, वह अब नहीं रही। विचार-स्वातंत्र्य और समयानुकूलता उनकी दृष्टि में अधर्म से कम नहीं। मैंने यह उपाय सोचा है कि किसी दूसरे शहर में चल कर अपना अड्डा जमाऊँ। मेरी वकालत भी यहॉँ नहीं चलती; इसलिए किसी बहाने की भी आवश्यकता न पड़ेगी।
मैं इस तजबीज के विरुद्ध कुछ न बोली। यद्यपि मुझे अकेले रहने से भय लगता था, तथापि वहॉँ स्वतन्त्र रहने की आशा ने मन को प्रफुल्लित कर दिया।
उसी दिन से अम्मॉँ ने मुझसे बोलना छोड़ दिया। महरियों, पड़ोसिनों और ननदों के आगे मेरा परिहास किया करतीं। यह मुझे बहुत बुरा मालुम होता था। इसके पहले यदि वह कुछ भली-बुरी बातें कह लेतीं, तो मुझे स्वीकार था। मेरे हृदय से उनकी मान-मर्यादा घटने लगी। किसी मनुष्य पर इस प्रकार कटाक्ष करना उसके हृदय से अपने आदर को मिटने के समान है। मेरे ऊपर सबसे गुरुतर दोषारोपण यह था कि मैंने बाबू जी पर कोई मोहन मंत्र फुर्क दिया है, वह मेरे इशारों पर चलते है; पर याथार्थ में बात उल्टी ही थी।
भाद्र मास था। जन्मष्टामी का त्यौहार आया था। घर में सब लोगों ने व्रत रखा। मैंने भी सदैव की भांति व्रत रखा। ठाकुर जी का जन्म रात को बारह बजे होने वाला था , हम सब बैठी गांती बजाती थी। बाबू जी इन असभ्य व्यवहारों के बिलकुल विरुद्ध थे। वह होली के दिन रंग भी खेलते, गाने बजाने की तो बात ही अलग । रात को एक बजे जब मैं उनके कमरे में गयी, तो मुझे समझाने लगे- इस प्रकार शरीर को कष्ट देने से क्या लाभ? कृष्ण महापुरूष अवश्य थे, और उनकी पूजा करना हमारा कतर्व्य है: पर इस गाने-बजाने से क्या फायदा? इस ढोंग का नाम धर्म नहीं है। धर्म का सम्बन्ध सचाई ओर ईमान से है, दिखावे से नहीं ।
बाबू जी स्वयं इसी मार्ग का अनुकरण करते थे। वह भगवदगीता की अत्यंत प्रशंसा करते पर उसका पाठ कभी न करते थे। उपनिषदों की प्रशंसा में उनके मुख से मानों पुष्प- बष्टि होने लगती थी; पर मैंने उन्हें कभी कोई उपनिषद् पढ़ते नहीं देखा। वह हिंदु धर्म के गूढ़ तत्व ज्ञान पर लट्टू थे, पर उसे समयानुकूल नहीं समझते थे। विशेषकर वेदांत को तो भारत की अबनति का मूल कारण समझाते थे। वह कहा करते कि इसी वेदांत ने हमको चोपट कर दिया; हम दुनिया के पदार्थो को तुच्छ समझने लगे, जिसका फल अब तक भुगत रहे हैं। अब उन्नति का समय है। चुपचाप बैठे रहने से निर्वाह नहीं। संतोष ने ही भारत को गारत कर दिया ।
उस समय उनको उत्तर देने की शक्ति देने की शक्ति मुझमें कहॉ थी ? हॉ, अब जान पड़ता है यह योरोपियन सभ्यता के चक्कर में पड़े हुए थे। अब वह स्वयं ऐसी बाते नहीं करते, वह जोश अब टंडा हो चला है।
इसके कुछ दिन बाद हम इलाहाबाद चेले आये। बाबू जी ने पहले ही एक दो- मंजिला मकान ले रखा था –सब तरह से सजा-सजाया। हमो यहाँ पॉच नौकर थे— दो स्त्रियाँ, दो पुरुष और एक महाराज। अब मैं घर के कुल काम-काज से छुटी पा गयी । कभी जी घबराता को कोई उपन्यास लेकर पढ़ने लगती ।
यहॉं फूल और पीतल के बर्तन बहुत कम थे। चीनी की रकाबियॉं और प्याले आलमारियों में सजे रखे थे । भोजन मेज पर आता था। बाबू जी बड़े चाब से भोजन करते। मुझे पहले कुछ शरम आती थी; लेकिन धीरे-धीरे मैं भी मेज ही पर भोजन करने लगी। हमारे पास एक सुन्दर टमटम भी थी। अब हम पैदल बिलकुल न चलते।
बाबू जी कहते – यही फैशन है ! बाबू जी की आमदनी अभी बहुत कम थी। भली-भांति खर्च भी न चलता था। कभी-कभी मैं उन्हें चिंताकुल देखती तो समझाती कि जब आया इतनी कम है तो व्यय इतना क्यों बढ़ा रखा है? कोई छोटो–सा मकान ले लो। दो नौकरों से भी काम चल सकता है। लेकिनं बाबू जी मेरी बातों पर हॅस देते और कहते–मैं अपनी दरिद्रता का ढिढोरा अपने-आप क्यों पीटूँ? दरिद्रता प्रकट करना दरिद्र होने से अधिक दु:खदायी होता है। भूल जाओं कि हम लोग निर्धन है, फिर लक्ष्मी हमारे पास आप दौड़ी आयेगी । खर्च बढ़ना, आवश्यकताओं का अधिक होना ही द्रव्योपार्जन की पहली सीढ़ी हैं इससे हमारी गुप्त शक्ति विकसित हो जाती हैं। और हम उन कष्टों को झेलते हुए आगे पंग धरने के योग्य होते हैं। संतोष दरद्रिता का दूसरा नाम है।
अस्तु, हम लोगों का खर्च दिन –दिन बढ़ता ही जाता था। हम लोग सप्ताह में तीन बार थियेटर जरूर देखने जाते। सप्ताह में एक बार मित्रों को भोजन अवश्य ही दिया जाता। अब मुझे सूझने लगा कि जीवन का लक्ष्य सुख –भोग ही है। ईश्वर को हमारी उपासाना की इच्छा नहीं । उसने हमको उत्तम- उत्तम बस्तुऍ भोगने के लिए ही दी हैं उसको भोगना ही उसकी सर्वोतम आराधना है। एक इसाई लेडी मुझे पढ़ाने तथा गाना सिखाने आने लंगी। घर में एक पियानो भी आ गया। इन्हीं आनन्दों में फँस कर मैं रामायण और भक्तमाल को भूल गयी । ये पुस्तकें मुझे अप्रिय लगने लगीं । देवताओं से विश्वास उठ गया ।
धीरे-धीरे यहॉ के बड़े लोगों से स्नेह और सम्बन्ध बढ़ने लगा। यह एक बिलकुल नयी सोसाटी थीं इसके रहन-सहन, आहार-व्यवहार और आचार- विचार मेरे लिए सर्वथा अनोखे थे। मै इस सोसायटी में उसे जान पड़ती, जैसे मोरों मे कौआ । इन लेडियों की बातचीत कभी थियेटर और घुड़दौड़ के विषय में होती, कभी टेनिस, समाचार –पत्रों और अच्छे-अच्छे लेखकों के लेखों पर । उनके चातुर्य ,बुद्धि की तीव्रता फुर्ती और चपलता पर मुझे अचंभा होता । ऐसा मालूम होता कि वे ज्ञान और प्रकाश की पुतलियॉ हैं। वे बिना घूंघट बाहर निकलतीं। मैं उनके साहस पर चकित रह जाती । मुझे भी कभी-कभी अपने साथ ले जाने की चेष्टा करती, लेकिन मैं लज्जावश न जा सकती । मैं उन लेडियों को भी उदास या चिंतित न पाती। मिसस्टर दास बहुत बीमार थे। परन्तु मिसेज दास के माथे पर चिन्ता का चिन्ह तक न था। मिस्टर बागड़ी नैनीताल में पतेदिक का इलाज करा रहे थे, पर मिसेज बागड़ी नित्य टेनिस खेलने जाती थीं । इस अवस्था में मेरी क्या दशा होती मै ही जानती हूं।
इन लेडियो की रीति नीति में एक आर्कषण- शाक्ति थी, जो मुझे खींचे लिए जाती थी। मै उन्हैं सदैव आमोद–प्रमोदक के लिए उत्सुक देखती और मेरा भी जी चाहता कि उन्हीं की भांति मैं भी निस्संकोच हो जाती । उनका अंग्रजी वार्तालाप सुन मुझे मालूम होता कि ये देवियॉ हैं। मैं अपनी इन त्रुटियों की पूर्ति के लिए प्रयत्न किया करती थीं।
इसी बीच में मुझे एक खेदजनक अनुभव होने लगा। यद्यपि बाबूजी पहले से मेरा अधिक आदर करते,मुझे सदैव ‘डियर-डार्लिग कहकर पूकारते थे, तथापि मुझे उनकी बातो में एक प्रकार की बनावट मालूम होती थीं। ऐसा प्रतीत होता, मानों ये बातें उनके हृदय से नहीं, केवल मुख से निकलती है। उनके स्नेह ओर प्यार में हार्दिक भावों की जगह अलंकार ज्यादा होता था; किन्तु और भी अचम्भे की बात यह थी कि अब मुझे बाबू जी पर वह पहले की –सी श्राद्धा न रही। अब उनकी सिर की पीड़ा से मेरे हृदय में पीड़ा न होती थी। मुझमें आत्मगौरव का आविर्भाव होने लगा था। अब मैं अपना बनाव-श्रृंगार इसलिए करती थी कि संसार में सह भी मेरा कर्तव्य है; इसलिए नहीं कि मैं किसी एक पुरूष की व्रतधारिणी हूँ। अब मुझे भी अपनी सुन्दरता पर गर्व होने लगा था । मैं अब किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए जीती थीं। त्याग तथा सेवा का भाव मेरे हृदय से लुपत होने लग था।
मैं अब भी परदा करती थी; परन्तु हृदय अपनी सुन्दरता की सराहना सुनने के लिए व्याकुल रहता था। एक दिन मिस्टर दास तथा और भी अनेक सभ्य–गण बाबू जी के साथ बैठे थे। मेरे और उसके बीच में केवल एक परदे की आड़ थी। बाबू जी मेरी इस झिझक से बहुत ही लज्जित थे। इसे वह अपनी सभ्यता में कला धब्बा समझते थे । कदाचित् यह दिखाना चाहते कि मेरी स्त्री इसलिए परदे में नहीं है कि वह रूप तथा वस्त्राभूषणों में किसी से कम है बल्कि इसलिए कि अभी उसे लज्जा आती है। वह मुझे किसी बहाने से बार-बार परदे के निकट बुलाते; जिसमें अनके उनके मित्र मेरी