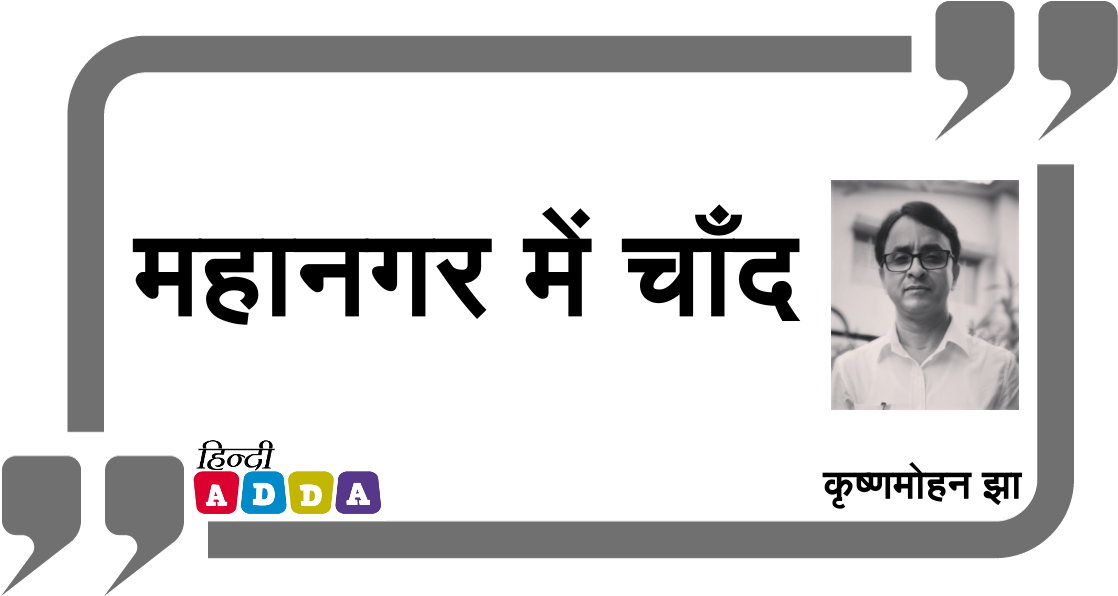महानगर में चाँद | कृष्णमोहन झा
महानगर में चाँद | कृष्णमोहन झा
महानगर में अपने चाँद को देखकर
मुझे उस पर रोना आता है
और शायद उसे भी अच्छा नहीं लगता इस हाल में मुझे पाकर
लगता है
पिछले जनम की बात है यह
जब कातिक की साँझ या बैसाख की रात में
चाँद और मैं
आँगन से दालान
और दलान से आँगन
इस प्रतियोगिता में भागते थे
कि देखें कौन पहुँचता है पहले
(और हर बार मैं हार जाता था उससे
क्योंकि उम्र में मुझसे काफी बड़ा था वह)
या फिर बाद के वर्षों में
जब मेरी हल्की-हल्की मूँछें निकल आईं थीं
और मेरे सीने में अक्सर दुखती हुई शाम
एक उदास आवारगी में लपेटकर मुझे यहाँ-वहाँ चली जाती थी
तब चाँद ही होता था मेरा सहचर
जिसके आत्मीय कंधे पर मैं रखता था अपना सर
लेकिन कुछ ही वर्षों बाद
हम दोनों ऐसे बिछड़े
जैसे ब्याह के बाद बिछुड़ती हैं
गाँव की जुड़वाँ बहनें
और उसका समाचार तभी-तभी पाया
जब ग्रहण ने उसे घेरा
जब दुख ने उसे खाया
और आज
इतने युगों बाद
जब हम हैं आमने-सामने
तो कातरता से रुँधा है मेरा गला
कुछ कहते बने न कुछ सुनते बने…
महानगर में
गुमशुदा की तलाश में निकले बड़े भाई सा जर्जर चाँद
चाँद का धूसर विज्ञापन लगता है
बस की खिड़की से बार-बार बाहर झाँकता हुआ मैं
लगता हूँ एक खोए हुए आदमी का विज्ञापन
धरती और आसमान से वंचित
त्रिशंकु की तरह
बीच में
लटका
हुआ
घर
उफ ! घर का कैसा विज्ञापन लगता है !