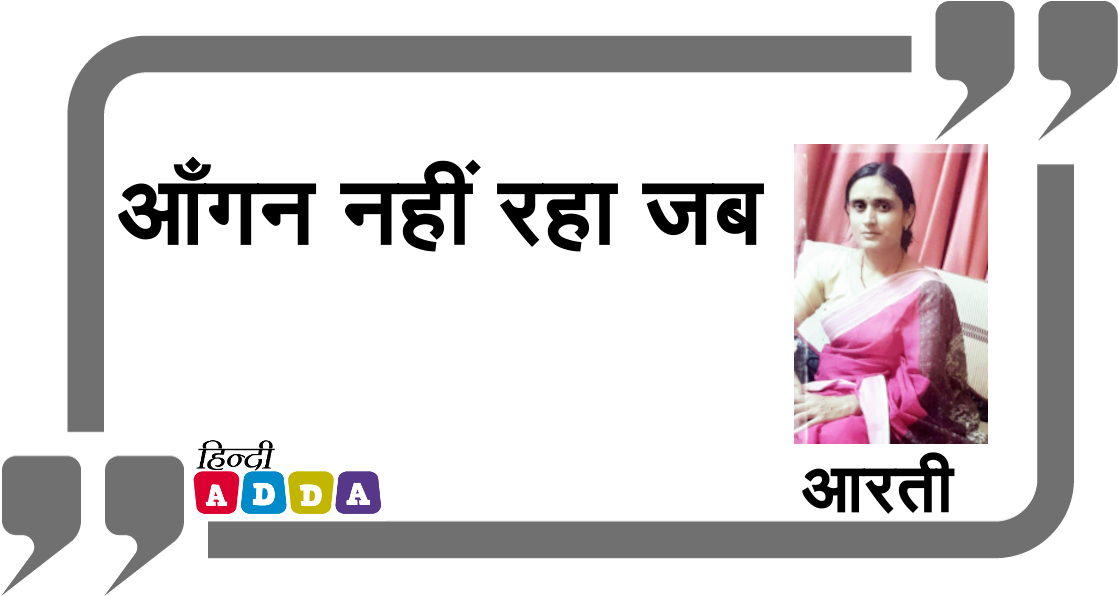आँगन नहीं रहा जब | आरती
आँगन नहीं रहा जब | आरती
आँगन इतना बड़ा तो न था
कि अँट जाए मन के कोनों में
दरारों में समा जाए
पर था
जैसे हवा होती है
जितनी चाहिए साँसों में भर लो
इसी तरह भर चुका था वह मेरे नथुनों में
शिराओं में धमनियों में
बस वहीं नहीं था आँगन, जहाँ था
दीवारों को बेधता
ओसारे दालान को लाँघता
फैल चुका था पड़ोस में
मोहल्ले में-खेत खलिहानों में
समूचे गाँव में
खुरदुरा अहसास उसका
हमारे तलवों की मालिश सा था
हम कूटते फटकते बीनते तो
आँगन गुनगुनाता संग साथ
हम सीते पिरोते तो वह
रोशनी की लकीरें खींचता
तबले की तीन ताल सा
तीनों पहर बजता रहता
कि पाँव पड़ते ही जमीन पर थिरकने लगते
कमोवेश हाथ की उँगलियाँ
पाँच-पाँच पाँव बन जातीं
वह पहचानता हमारे चेहरे के मनोभाव
अलसाई देह और जहाइयाँ गिनकर
घड़ी की सुइयों सी आवाज लगा देता
‘दिन डूब रहा है’
पहले दिये का हकदार वही तो था
आँगन जमीन का एक टुकड़ा न था
वह धूप
पहली बारिश
जेठ की शाम
और खुली साँस लेने का एक मौका था
जायदाद नहीं था वह
जैसा कि दो भाइयों ने माना
रिश्तों में बिचबैया की भूमिका निभाता वह
आज, बँटवारे की दीवार वजूद पर लादे खड़ा है
पहली बार जाना
सीमाएँ आँगन में भी होती हैं
अब आँगन नहीं रहा तो
नहीं रहे आमों में बौर
गिलहरियों के ठौर भी नहीं रहे
नहीं रहे किस्से और गीत
पता नहीं चाँद तारे रहे या नहीं
किसी प्रेतात्मा सा आँगन
मुझ पर काबिज हो
जीत के पाँसे फेंक चुका है
चेतना के चौथाई हिस्से में घुल चुका
अब वह अंश मात्र नहीं है
आँचल हिलाती मेरा, सर्र सर्र बहती रही हवाएँ
जलतरंग सी बजतीं क्रियाएँ
और तलवों की शिराएँ
दीवारों को तोड़ आँगन की ओर
दौड़ जाना चाहती हैं