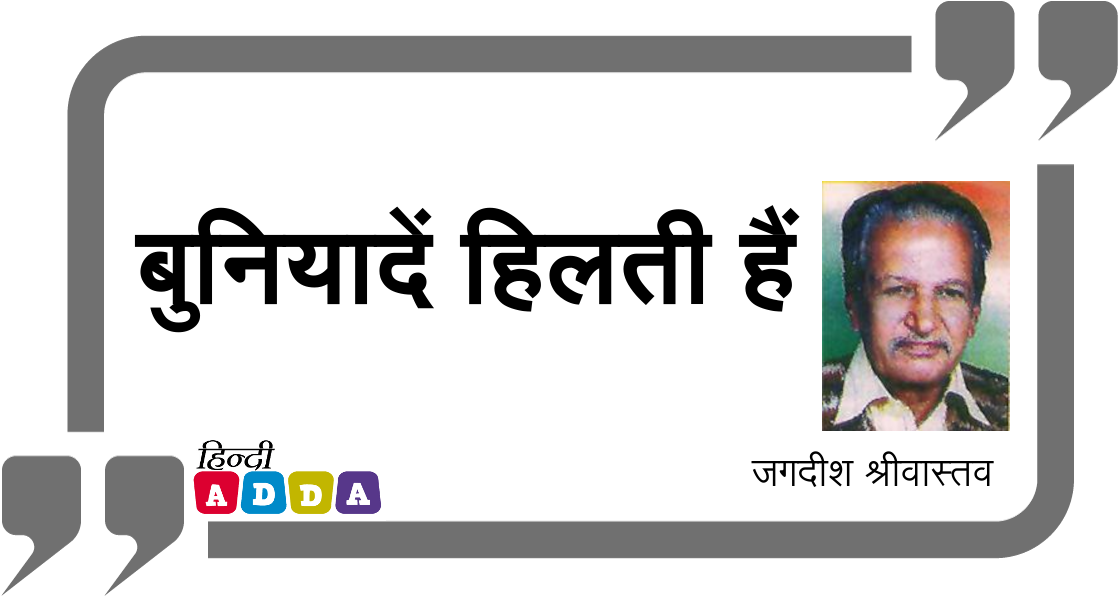बुनियादें हिलती हैं | जगदीश श्रीवास्तव
बुनियादें हिलती हैं | जगदीश श्रीवास्तव
बाहर का कोलाहल
भीतर का अंधियारा
हर दिन ही डसता है सूनापन हमको फिर
बाँहों में कसता है।
अपनों का दर्द लिए
घिर गए सवालों में
तने हुए चेहरों के बीच से गुजरना है
हाथ की लकीरों ने
इस तरह काटा है
आग की नदी में अब रोज उतरना है
मंजिल है पास बहुत फिर भी मजबूरी है
राहों का अंधियारा बार-बार डसता है।
गली सड़क चैराहे
दीवारें गुम सुम हैं
प्यास यहाँ खूँटी पर रोज ही लटकती हैं
भीड़ भरे शहरों में
आदमी अकेला है
लावारिश सड़कों पर रोशनी भटकती है
धुआँ जलन खामोशी आँखों में सपने हैं
जाने क्यूँ सन्नाटा मुझ पर ही हँसता है।
जिंदगी किताबों के
पन्नों-सी बिखरी है
खिड़की के साथ यहाँ उखड़े दरवाजे हैं
अपना ही बोझ लिए
बुनियादें हिलती है
सर्दियों के कंधों पर वक्त के तकाजे हैं
चक्रव्यूह जीवन को हर दिन ही कसता है
कैद हुए घर में हम सूनापन डसता है।