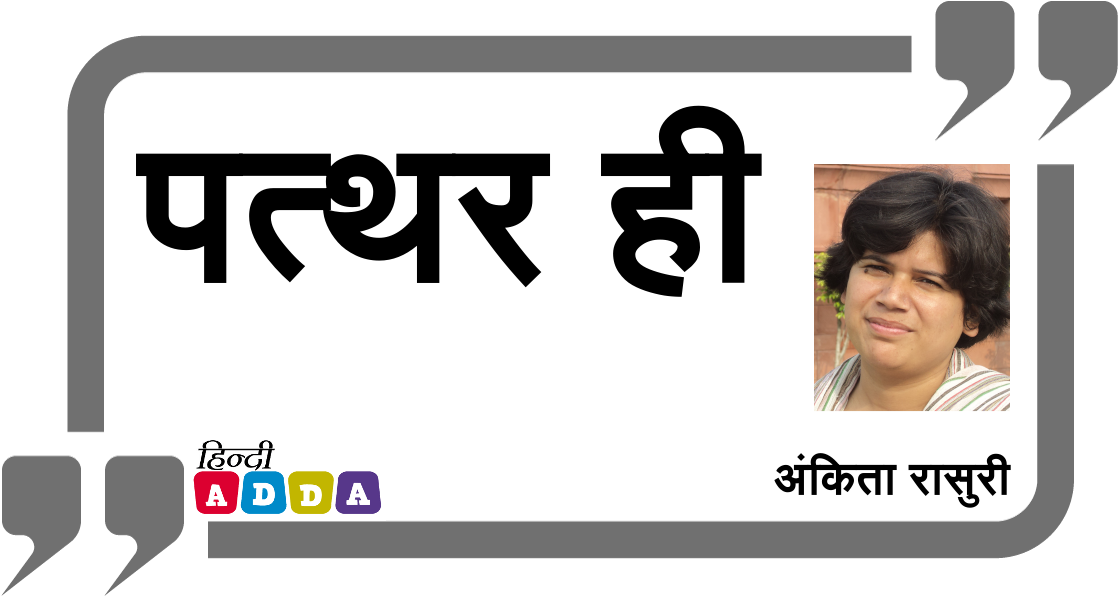पत्थर ही | अंकिता रासुरी
पत्थर ही | अंकिता रासुरी
जंगल के किसी छोर में विस्तृत घास पर लेटी हुई
दूर-दूर तक निहारती हूँ
घाटी में बहती हुई नदी को
उसका सरसराहट वाला मंद स्वर
सुनना व समझना चाहती हूँ
विस्तृत होते हुए दरख्तों से चाहती हूँ
उसकी टहनियों को आगोश में सोती रहूँ निरंतर
पत्तियों के झुरमुटों से दिखते बिखरे रंगीन बादलों को
उँगलियों के पोरों से छूकर
उनकी नमी का राज पा लेना चाहती हूँ
पर ये क्या
मेरा हृदय इतना संवेदनहीन क्यों हो गया है
कुछ तो महसूस करे
हाँ कुछ एहसासों को बर्फ बना देना चाहा था हृदय ने
जो भीतर ही भीतर बहा करते थे किसी त्रासदी की तरह
सब कुछ जम जाएगा उन एहसासों के साथ
ये कहाँ जाना था
मेरी उदासीनता भरी इस छटपटाहट को अब ये मूक पत्थर ही समझ सकते हैं